VSK Bharat
मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अथवा मनुष्य अपने सामने जीवन का लक्ष्य कौन सा रखे? इस बारे में लगभग सभी लोगों का मत है कि सुख ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। परंतु, प्रश्न यह है कि सुख से आशय क्या है और मनुष्य को यह सुख कैसे मिल सकता है?
इस सम्बन्ध में श्री गुरुजी के अनुसार पश्चिमी चिन्तन और हिन्दू दर्शन पर आधारित भारतीय चिन्तन में मूलभूत अन्तर है। इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए श्री गुरुजी ने अनेक प्रकार से समझाया है कि सुख के बारे में पश्चिमी विचार अधूरा, एकांगी, अस्थायी एवं क्षणभंगुर है, वस्तुतः तो वह सुख का क्षणिक आभास देते हुए अन्ततः दुखकारी ही है। इसके विपरीत सुख की हिन्दू परिकल्पना समग्र, संतुलित एवं अधिक स्थायी है।
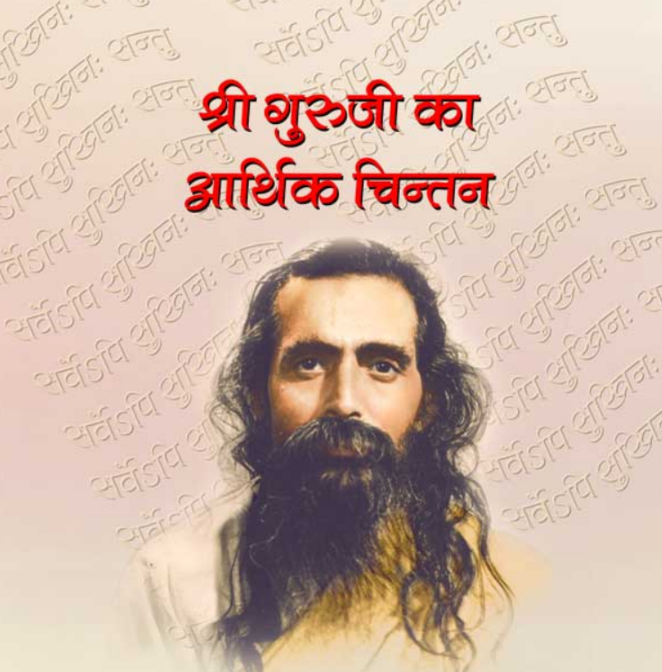
पश्चिमी राष्ट्रों का लक्ष्य – केवल भौतिक सुख
पश्चिमी राष्ट्रों ने सुख की परिकल्पना केवल भौतिक एवं ऐहिक सुख के रूप में ही की है। इस सम्बन्ध में श्री गुरुजी ने कहा है – ‘‘दुनिया भर की राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्र व्यवस्था में मनुष्य मात्र के जीवन का लक्ष्य ऐहिक सुख समृद्धि माना हुआ है। अर्थात् खाना-पीना, वस्त्र प्रावरण, निवास के स्थान, सुखोपभोग, वासना की वृद्धि, वासना संतुष्ट करने के साधनों की वृद्धि, उन साधनों की उपलब्धि, भिन्न-भिन्न मनोविनोद के साधन, यही जगत के सब देशों में सर्वसाधारण लक्ष्य रखा गया है, ऐसा दिखता है। जिसका बड़ा प्रगतिमान वर्णन किया जाता है, वहाँ सामान्य आदमी के यहाँ भी टेलीविजन, रेडियो, मोटर, मोटर साइकिल आदि ऐहिक सुख के लक्षण ही प्रगति के मापदण्ड माने जाते हैं। पर ये वास्तव में मानव की प्रगति के मापदण्ड हैं क्या?’’
भौतिक सुख की यह अवधारणा अधूरी है और यह अंततोगत्वा असंतोष, अशान्ति एवं संघर्ष का ही कारण बनती है, इस बात पर श्री गुरुजी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को सुख की प्राप्ति करवा देने का ध्येय सामने रखकर चलने का दावा करने वाली बहुत सी जीवन रचनाएं आज संसार में विद्यमान हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति में ही सुख है, इसी बात को लेकर अनेक आधुनिक विचार प्रणालियाँ उत्पन्न हुई हैं। परन्तु कुछ काल के लिए होने वाली वासनापूर्ति आगे चलकर मनुष्य को अशान्त करती हुई दिखाई देती है।
श्री गुरुजी के अनुसार इसके कई कारण है –
(1) एक तो विषय वासनाओं की पूर्ति सर्वथा असम्भव है। उनको तुष्ट करने की जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही वे बढ़ती हैं। ‘‘अनुभव यह बताता है कि मनुष्य दैहिक आनन्द प्राप्त करने का जितना अधिक प्रयास करता है, उसकी भूख उतनी ही तीव्र होती जाती है। उसे कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। इच्छाओं के तुष्टिकरण की चेष्टा जितनी अधिक होगी, उतना ही असंतोष बढे़गा। भौतिक सुख साधनों का संग्रह करने की इच्छा जितनी ही प्रबल होगी, निराशा भी उतनी अधिक होगी। हमारे शास्त्रों ने घोषणा की है – ‘न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति’ (महा0 आदिपर्व)। विषय भोगों से कामनाओं का शमन नहीं होता। शरीर के जीर्णशीर्ण हो जाने पर भी इच्छाएं पूर्ववत् युवा बनी रहती हैं। भर्तृहरि ने भी कहा है – ‘तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः’ (वैराग्य शतक) – यही वास्तविक दुर्दशा है, जिसमें आधुनिक मानव स्वयं को फँसा हुआ पाता है। इस प्रकार वासनापूर्ति असम्भव होने के कारण मानव जीवन दुःखी होता हुआ दिखाई देता है।
(2) भौतिक पदार्थों से अपनी वासनापूर्ति में लगे मनुष्य को प्रारम्भ में भले ही कुछ संतुष्टि मिले पर, ‘‘आगे चलकर वह समझ जाता है कि इन आपाततः सुख देने वाली वस्तुओं में वास्तविक सुख देने की कोई शक्ति नहीं है। सुख तो अपने ही अन्दर समय-समय पर उठने वाली वासना-तंरगों की शांति से होता है। यानि सुख बाह्य वस्तु में नहीं, वासना पूर्ति में भी नहीं; किन्तु वासना के शांत होने में है।’’
(3) श्री गुरुजी का मानना था कि ‘‘व्यक्ति व समाज के लिए वासनाओं का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना और उस पर सदा असंतोष का बना ही रहना, यही जगत में बार-बार होने वाले भयंकर युद्धों का प्रमुख कारण है। जगत में अशांति तथा असुख बनाएं रखने में, यही प्रबल कारण है।’’
श्री गुरुजी ने इसी बात को विस्तार से समझाया है, कहा है कि – ‘‘पश्चिम के सुख की अवधारणा पूर्णतया प्रकृतिजन्य इच्छाओं की संतुष्टि पर ही केन्द्रित है, अतः उनके ‘जीवन स्तर को उठाने’ का अर्थ भी केवल भौतिक आनन्द की वस्तुओं को अधिकाधिक जुटाना है। इससे व्यक्ति अन्य विचारों एवं एषणाओं को छोड़कर केवल इसी में पूर्णतया संलग्न हो जाता है। भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति की इच्छा धन-संग्रह को जन्म देती है। अधिकाधिक धन प्राप्ति हेतु शक्ति आवश्यक हो जाती है; किन्तु भौतिक सुख की अतृप्त क्षुधा व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीय सीमाओं तक ही नहीं रुकने देती। सबल राष्ट्र राज्य शक्ति के आधार पर दूसरों के दमन व शोषण का भी प्रयास करते हैं। इसमें से संघर्ष व विनाश का जन्म होता है। एक बार यह प्रक्रिया प्रारम्भ हुई कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। सभी नैतिक बंधन विच्छिन्न हो जाते हैं। सामान्य मानवीय संवेदनाएं सूख जाती हैं। मनुष्य और पशु में अन्तर स्थापित करने वाले मूल्य एवं गुण समाप्त हो जाते हैं।’’